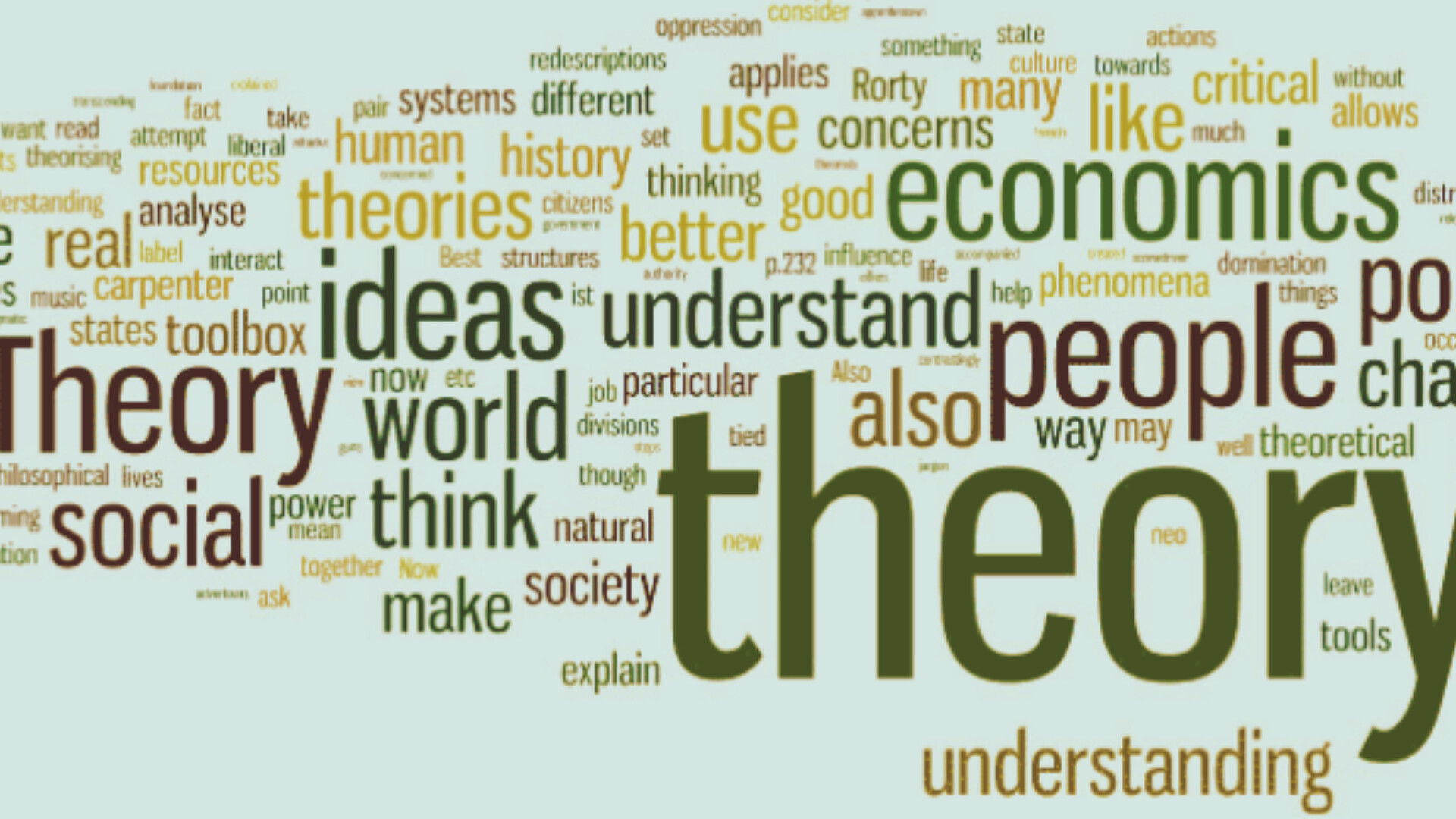
अपनी बात, विचार और सूचना को साझा करने के लिए मीडिया यानी माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। मीडिया आधुनिक युग में सूचना, संवाद और मनोरंजक के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। जिसने लोगों को अपने हर रूप चाहे वह प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर डिजिटल हो से लोगों के दिलों को जीता है। आज हर ओर मीडिया के गुणगान सुनाए देते हैं। वहीं मीडिया की लोकप्रियता के चलते मीडिया सिद्धान्त शब्द जन्म हुआ है। अतः मीडिया सिद्धान्त से तात्पर्य है कि मीडिया कैसे काम करता है, उसका प्रभाव क्या है और वह कैसे व्यक्तियों, समाज, संस्कृति और राजनीति के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करता है।
मीडिया सिद्धान्तों का विकास अलग-अलग समय पर हुआ और सिद्धान्त अपने अलग दृष्टिकोण, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर केंद्रित है। मीडिया सिद्धान्तों की विशेषता यह है कि ये मीडिया की प्रकृति और प्रभावों का विश्लेषण करते हैं साथ ही इस बात की व्याख्या भी करते हैं कि कैसे व्यक्ति, समाज, दर्शक, पाठक और श्रोता मीडिया विषयवस्तु को ग्रहण करते हैं।
इस आर्टिक्ल में हम मीडिया सिद्धान्तों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि मीडिया सिद्धान्त किस तरह मीडिया अध्ययन और शोध के लिए एक आधारशिला का काम करते हैं।
प्रमुख मीडिया सिद्धान्तों की सूची-
| मीडिया सिद्धान्त (Media Theories) | वर्ष (Year) | प्रतिपादक (Founder) | प्रमुख बिंदु (Key Points) |
| 1. प्रोपोगेंडा के आधारभूत सिद्धान्त | 1925 | डूब | |
| 2. अरस्तू का मॉडल | अरस्तू | ★अरस्तू का संचार मॉडल सबसे पुराने और प्रभावशाली संचार मॉडलों में से एक है। ★ अरस्तू मॉडल को रिटोरिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकिं यह प्रभावशाली भाषण और संवाद पर केंद्रित है। ★ अरस्तू के मॉडल में 3 प्रमुख तत्व शामिल हैं- 1. वक्ता (Speaker) 2. सन्देश (Speech/Message) 3. श्रोता (Audience) ★ अरस्तू का मॉडल इस बात पर जोर देता है कि संचार का उद्देश्य श्रोता को प्रभावित करना और उन्हें किसी कार्य, विचार या व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। ★ अरस्तू का मॉडल सन्दर्भ (Context) और अवसर (Occasion) पर भी केंद्रित है। ★ अरस्तू ने प्रभावशाली संचार के लिए तीन साधन बताएं हैं- 1. एथोस (Ethos)- वक्ता की विश्वसनीयता और नैतिकता। 2. पैथोस (Pathos)- श्रोता की भावनाओं को प्रभावित करना। 3.लोगोस (Logos)- तर्क और तथ्य का उपयोग। ★ अरस्तू का मॉडल एकतरफा संचार मॉडल है जिसमें केवल वक्ता सक्रिय होता है और श्रोता निष्कर्ष। ★ इस मॉडल का उद्देश्य श्रोता को प्रेरित करना और उनकी राय या दृष्टिकोण को बदलना है। ★ यह सिद्धांत केवल औपचारिक और सार्वजनिक संचार के लिए उपयुक्त है। ★ इसमें श्रोता की प्रतिक्रिया (Feedback) का अभाव पाया जाता है। | |
| 3. हेरोल्ड डी लॉसवेल का मॉडल | 1948 | हेरोल्ड डी लॉसवेल | ★ हेरोल्ड डी लॉसवेल के सिद्धान्त को “लॉसवेल का सूत्र” नाम से भी जाना जाता है। ★ लॉसवेल ने अपने सिद्धान्त में 5 तत्वों का वर्णन किया है जो कि सवालों के रूप में हैं। वे हैं- 1. कौन? 2. क्या कहता है? 3. किस माध्यम से? 4. किसे? 5. क्या प्रभाव पड़ता है? ★ लॉसवेल ने अपने मॉडल में लक्ष्य और प्रभाव पर जोर दिया है। ★ लॉसवेल का मॉडल सीधा और रेखीय मॉडल है। जिसमें संचार एक ही दिशा की ओर होता है। उदाहरण के लिए, संचारकर्ता से श्रोता की ओर। ★ इस मॉडल में यह महत्वपूर्ण है कि सन्देश को किस माध्यम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। ★ इस मॉडल का उपयोग मुख्यतः जनसंचार, राजनीति और प्रसार के क्षेत्र में किया जाता है। ★ यह मॉडल श्रोता की प्रतिक्रिया तथा पारस्परिक संवाद पर ध्यान नहीं देता। ★ मॉडल का स्वरूप रेखीय होने के कारण यह जटिल संचार प्रक्रियाओं को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। |
| 4. चार्ल्स ऑसगुड का मॉडल या कोंग्रिटी मॉडल | 1954 | चार्ल्स ऑसगुड | ★ चार्ल्स ऑसगुड के मॉडल को कोंग्रिटी मॉडल के नाम से जाना जाता है। ★ यह मॉडल मुख्य रूप से दृष्टिकोण परिवर्तन दृष्टिकोण परिवर्तन और संप्रेषण के प्रभाव को समझाने के लिए बनाया गया है। ★यह मॉडल ऑडिएंस के विचार और भावनात्मक जुड़ाव को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में मदद करता है। ★ इस मॉडल के अनुसार दृष्टिकोण परिवर्तन के दो कारण होते हैं- 1. सन्देश का स्रोत (Source) 2. विषय (Object) ★ स्रोत और विषय के प्रति व्यक्ति की धारणा परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ★ चार्ल्स ऑसगुड ने अपने सिद्धान्त में सिमेंटिक डिफरेंशियल तकनीक का भी उपयोग किया। ★ ऑसगुड का सिद्धांत यह बताता है कि लोग ऐसे विचार या दृष्टिकोण को अपनाना अधिक पसंद करते हैं जो उनमें पहले से मौजूद विचारों या विश्वासों से मेल खाते हों। |
| 5. हेलिकल मॉडल या डांस का वर्तुल मॉडल | 1967 | ई. एक्स डांस | ★ डांस का मॉडल संचार की एक स्पाइरल प्रक्रिया है। जो कि गोल-गोल घूमती हुई सीढ़ी या स्पाइरल की तरह निरन्तर आगे बढ़ती रहती है।जिसका अर्थ है कि संचार कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है तथा यह समय के साथ और भी विकसित होती जाती है। ★ हेलिकल मॉडल यह कहता है कि संचार कभी खत्म नहीं होता। यह समय, अनुभव और अभ्यास से बेहतर होता जाता है। |
| 6. विल्बर श्राम का मॉडल | 1954 | विल्बर श्राम | ★ विल्बर श्राम का मॉडल एक चक्रीय प्रक्रिया या दोतरफा प्रक्रिया है। अतः यह मॉडल बताता है कि संचार केवल भेजने तक सीमित न होकर प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया भी बताता है। इस प्रकार यह एक पूर्ण चक्र बनाता है। ★यह मॉडल बताता है कि संचार तबतक अधूरा है जब तक प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त न हो जाये। ★ संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच अनुभव और सन्दर्भ का क्षेत्र का मेल होना जरूरी है। ★ यह मॉडल बताता है कि संचार की प्रक्रिया स्थिर न होकर एक गतिशील और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। |
| 7. जॉर्ज गर्बनर का मॉडल | 1956 | जॉर्ज गर्बनर | ★ जॉर्ज गर्बनर के मॉडल को जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ★ गर्बनर मॉडल में संचार प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। 1. इवेंट 2. मेसेज 3. सेंडर/एनकोडर ★इस मॉडल के अनुसार सन्देश को समझने की प्रक्रिया दर्शकों की धारणा पर निर्भर करती है। ★गर्बनर का मॉडल मुख्य रूप से जनसंचार पर केंद्रित है। जिसमें अक्सर प्रतिक्रिया की कमी होती है। ★ गर्बनर का मॉडल एक तरफा संचार को बेहतर तरीके से समझाता है। ★ यह मॉडल बताता है कि संचार स्थिर न होकर एक गतिशील और निरन्तर प्रक्रिया है। |
| 8. जॉर्ज गर्बनर का संशोधित मॉडल | 1967 | जॉर्ज गर्बनर | ★गर्बनर के संशोधित मॉडल को 2 स्तरों में बांटा गया है। स्तर एक में सन्देश का निर्माण, प्रसारण, स्रोत द्वारा घटना का चयन और प्रतिनिधित्व शामिल हैं। वहीं स्तर 2 में शामिल है- दर्शकों पर सन्देश का प्रभाव और व्याख्या। |
| 9. सनतांत्रिक सिद्धान्त या संचार का गणितीय सिद्धान्त या सूचना सिद्धान्त | 1949 | क्लाउड शैनन और वारेन वीवर | ★ शैनन वीवर मॉडल संचार प्रक्रिया को 6 तत्वों में विभाजित करता है। जो हैं- 1. स्रोत 2.सन्देश 3. प्रेषक 4.संचार माध्यम 5.शोर 6.प्राप्तकर्ता ★ इस सिद्धान्त में सूचना को मापने के लिए बिट का उपयोग किया जाता है। ★ यह मॉडल मुख्य रूप से तकनीकी और तार्किक संचार (टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट) पर केंद्रित है। |
| 10. सन्तुलन सिद्धान्त (Balance Theory) | 1946 | फ्रिट्ज हैदर | |
| 11. ए बी एक्स मॉडल | 1953 | मैक्सवेल न्यूकॉम्ब | |
| 12. वेस्ली और मैकलीन का मॉडल | 1957 | वेस्ली और मैकलीन | |
| 13. सन्तुलन और सामंजस्य का सिद्धांत (Balance and Congruity Theory) | 1946-1958 | हाइडर | |
| 14. सम्मिति का सिद्धांत | 1953 | न्यूकॉम्ब | |
| 15. अनुरूपन का सिद्धांत | 1955 | ऑसगुड और टेननबोम | |
| 16. ज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत | 1957 | फेस्टिनजर | |
| 17.सात्यता का द्विप्रक्रिया सिद्धांत | 1966 | मेकग्यूरी (Acquire) | |
| 18. अभिप्रेरणा का सिद्धांत | 1939 | कॉटज़ और स्टोटलैंड | |
| 19. सामंजस्य सिद्धान्त (Congruity Theory) | 1955 | ऑसगुड और टोनेनबॉम | |
| 20. संचार का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत (Perceptual theory of communication) | हॉवार्ड जाइल्स | ||
| 21. संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धान्त (Cognitive Dissonance Theory) | 1987 | फेसस्टिंगर | |
| 22. भावनात्मक संज्ञानात्मक संगति सिद्धान्त (Affective Cognitive Consistency Theory) | 1960 | रोजेनबर्ग | |
| 23. चर्चावाली निर्धारण सिद्धान्त (Agenda Setting Theory) | 1972 | मैक्सवेल ई. मेकॉम्ब एवं डोनाल्ड एल. शा | |
| 24. उपयोगिता एवं परितुष्टि का सिद्धांत (Uses and Gratification theory) | एलियाह काट्ज़, जे. ब्लूमर और माइकल गर्विच | ||
| 25. छवि विकास सिद्धान्त (Cultivation Theory) | 1973 | गेर्बनर | |
| 26. निर्भरता का सिद्धान्त (Dependancy theory) | 1976 | बॉल रोकिक और डी फ्लोयर | |
| 27. बुलेट सिद्धान्त या प्रेषण दृष्टि या ह्यपोडर्मिक नीडल थ्योरी | 1920-1930 | ||
| 28. मार्शल मैकलुहान का सिद्धांत | 1962 | मार्शल मैकलुहान | |
| 29. द्विपद एवं बहुपद सिद्धान्त (Two steps and multi steps theory) | 1955 | काट्ज़ और लाजर्सफील्ड | |
| 30. मौन का वलय (The spiral of silence) | 1973-80 | एलिजाबेथ नोबेल न्यूमैन | |
| 31. सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धान्त | 1940 | रॉबर्ट हटकीन्स की अध्यक्षता में। | |
| 32. प्रजातांत्रिक-प्रतिभागिता मीडिया सिद्धान्त | 1960-70 | डेनिस मैक्वेल | |
| 33. संचारण का सिद्धान्त (Diffusion of innovation theory) | 1962 | एवरेस्ट एम रोजर्स | |
| 34. प्रत्यायन और अभिवृत्ति परिवर्तन सिद्धान्त (Attribution and attitude change theory) | 1958 | फ्रिट्ज हाइडर | |
| 35. अभिसरण और वैविध्य का सिद्धांत (Convergance and divergence Theory) | 1974 | जॉन डी. कास्टर और मार्गरेट जानोवित्ज़ | |
| 36. संचार का अभिसरण सिद्धान्त (Convergence theory of communication) | 1979 | लॉरेंस किंकेड | |
| 37. कला और विज्ञान | 1971 | नोरा सी क्यूब्रल | |
| 38. जादुई गुणक या मैजिक मल्टीप्लायर | 1964 | विल्बर श्रैम | |
| 39. प्रबंधन के तत्व (Elements of management) | 1916 | हेनरी फेयोल | |
| 40. व्यवसायीकरण सिद्धान्त (Commercialization Theory) | एफ. रोज़ारियो ब्रेड | ||
| 41. तदनुभूति (Empathy) | कार्ल रोजर्स | ||
| 42. मॉडर्नाइजेशन सिद्धान्त | 1958 | डेनियल लर्नर | |
| 43. तमाशा या स्पेक्टेकल सिद्धान्त | 1967 | गाय डिबोर्ड | |
| 44. कर्तव्यशास्त्रीय सिद्धान्त या डियोंटोलॉजिकल थ्योरी | इमेनुएल कांट | ||
| 45. ढांचा विश्लेषण का सिद्धांत | 1974 | इर्विंग गोफमैन | |
| 46. दृश्य प्रस्तुति सिद्धान्त (The presentation of self in everyday life theory) | 1959 | इरविंग गोफमैन | |
| 47. सामाजिक विकास का सिद्धांत | डेविड मूर और विलियम एच. रोजर्स | ||
| 48. सामाजिक विकास का चरण सिद्धान्त (Stages of social development theory) | कुलबर्ट रॉस | ||
| 49. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सिद्धान्त | 1978 | एडवर्ड सईद | |
| 50. सांस्कृतिक क्षेत्रीयता का सिद्धांत (Cultural Regionalism theory) | डी. आर मानकेकर | ||
| 50. सीमित प्रभाव सिद्धान्त (Limited Effects theory) | 1940-50 | एल्विन गोल्डबर्ग और पॉल लाजरसफील्ड | |
| 51. पी.आर का पिरामिड मॉडल | 1984 | जेम्स ई. ग्रुनिंग और टॉड हंट | |
| 52. मापन और मूल्यांकन का बहुआयामी मॉडल (Multi Dimensional Model of Evaluation and Measurement Model) | 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत | जिम मैकनेमारा | |
| 53. प्रभावपूर्ण मानदण्ड मॉडल (Excellence theory of public relations) | 1980-90 | जेम्स ई. ग्रुनिंग | |
| 54. अल्पकालिक एवं सतत मॉडल | 1997 | वॉटसन | |
| 55. व्यवहारवाद का सिद्धांत | 1913 | जॉन. बी. थॉम्पसन | |
| 56. प्रीपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पेक्ट मॉडल | 1985 | कटलिप, सेंटर और ब्रूम | |
| 57. जनसंपर्क प्रबंधन प्रक्रिया मॉडल | 1985 | कटलिप, सेंटर और ब्रूम | |
| 58. जनसम्पर्क के चार रोल मॉडल (Four roles of public relations practitioners) | 1985 | कटलिप, सेंटर और ब्रूम | |
| 59. थ्री स्टेप यारडिस्टिक मॉडल | 1993 | वॉल्टर लिंडरमैन | |
| 60. पिरामिड मॉडल या मानव आवश्यकताओं का पिरामिड | 1943 | अब्राहम मास्लो | |
| 61. टेलीविजन के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक प्रारूप | 1972 | एलियट एल. आर्लबैक | |
| 62. प्रेरणा सिद्धान्त (Field theory) | कुर्ट लेविन | ||
| 63. प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक लगाव सिद्धान्त | जॉन बोल्बी और मैरी एनस्वर्थ | ||
| 64. शहरी विरुद्ध ग्रामीण समाज | एम्मिल दुर्ख़ाइम | ||
| 65. जेमेंशाफ्ट विरुद्ध जेसेलशाफ्ट | 1887 | फर्डिनेंड टोनिस | |
| 66. पारंपरिक विरुद्ध आधुनिक समाज | मैक्स वेबर | ||
| 67. विकासात्मक माध्यम सिद्धान्त | 1984 | मैक्वेल | |
| 68. केंद्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत सन्देश | कर्ट लेविन और एडगर शीन | ||
| 69. सोवियत मीडिया सिद्धान्त | कार्ल मार्क्स और ऐंगल्स | ||
| 70. विकासात्मक अध्ययन सिद्धान्त | एवरिट रोजर और क्लॉड एलेन | ||
| 71. प्रदर्शक समाज सिद्धांत | सिल्वियो गैस्सेल | ||
| 72. मध्यस्थ अतिवास्तविकता (HyperReality) | ज्यां बौद्रियर | ||
| 73. एंट्रोपी | शैनन एन्ड वीवर | ||
| 74. ग्रोथ थ्योरी | वॉल्ट रोस्तोव | ||
| 75. रिप्रेजेंटेशन | स्टुअर्ट हॉल | ||
| 76. मेलगेज | जोएल बेरेल्सन और नॉर्मन बर्नार्ड |
मीडिया क्षेत्र में मीडिया सिद्धान्त अहम भूमिका निभाते हैं। यह न केवल समाज, संस्कृति और व्यवहार को प्रभावित करते हैं बल्कि इनका उपयोग जनमत निर्माण, सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रेरित करने और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है।
मीडिया सिद्धान्त एकेडमिक शोध के साथ-साथ मीडिया पेशेवरों, नीति निर्माताओं और आम लोगों के लिए भी उपयोगी हैं। सिद्धान्त का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है। अतः ये परिदृश्य को समझने और भविष्य के लिए प्रभावी रणनीतियों का निर्माण भी करते हैं।
मीडिया सिद्धान्त समाज और मीडिया के बीच परस्पर प्रभाव को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये मीडिया सिद्धान्तो का अध्ययन हमें एक जागरूक और सतर्क मीडिया उपभोक्ता बनने के लिए प्रेरित करता है।